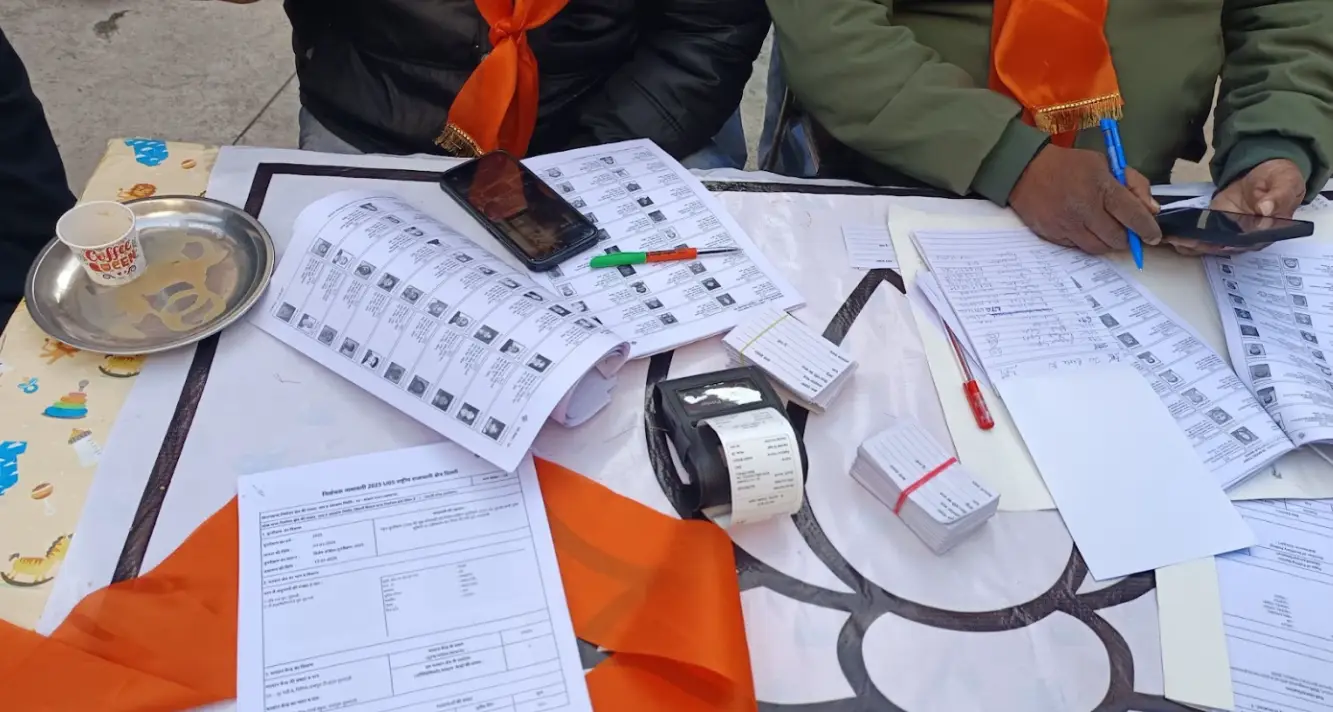एग्जिट पोल | Exit Poll – A Complete Analysis
लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और भविष्यवाणियाँ कोई नई बात नहीं हैं। दुनिया भर में चुनावी अध्ययन लंबे समय से सामाजिक विज्ञानों में शोध के उद्देश्य से किए जाते रहे हैं। भारत में Exit Poll के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत में पहला चुनावी सर्वेक्षण “इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन” के द्वारा किया गया था। यह 1957 में हुए दूसरे लोकसभा आम चुनाव के दौरान हुआ था। इस सर्वेक्षण का नेतृत्व एरिक डी कोस्टा ने किया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से एक्ज़िट पोल नहीं कहा जा सकता।
बाद के वर्षों में में, 1980 में, डॉ. प्रणय रॉय और अशोक लाहिड़ी ने इंडिया टुडे पत्रिका के लिए पहला एक्ज़िट पोल किया, जिसे उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में भी दोहराया। 1996 में, दूरदर्शन द्वारा एक्ज़िट पोल किया गया था। इस सर्वेक्षण का संचालन पत्रकार नलिनी सिंह ने किया, और डेटा संग्रह का कार्य सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (CSDS) ने किया।
इसी तरह यदि हम पूरी दुनिया की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला एक्ज़िट पोल 1936 में हुआ था। यह सर्वेक्षण जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन के द्वारा न्यूयॉर्क शहर में किया गया, जिसमें उन्होंने मतदान केंद्र से बाहर आते मतदाताओं से पूछा कि उन्होंने किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट दिया। इस डेटा के विश्लेषण के आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी की कि फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट चुनाव जीतेंगे, और यह भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। इसके बाद, अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी एक्ज़िट पोल लोकप्रिय हो गए। ब्रिटेन में पहला एक्ज़िट पोल 1937 में और फ्रांस में 1938 में हुआ।
भारत में, टेलीविजन और बाद में इंटरनेट के आगमन ने एक्ज़िट पोल के उद्देश्यों को बदल दिया है। पहले केवल शोध के उद्देश्य से किए जाने वाले चुनावी सर्वेक्षण अब मुख्य रूप से चुनावी भविष्यवाणी और सीटों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किए जाने लगे हैं। जैसे-जैसे एक्ज़िट पोल का प्रभाव बढ़ा, यह शोध-आधारित अध्ययन से एक प्रकार के मनोरंजन में बदल गया। अब एक्ज़िट पोल की लोकप्रियता बनाए रखने का भी दबाव बढ़ गया है। हाल के वर्षों में कई एक्ज़िट पोल गलत साबित हुए हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। यदि हम ऐसे चुनावों की बात करे जब एग्जिट पोल गलत साबित हुए तो इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल, 2004 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल, हरियाणा 2024 चुनाव के एग्जिट पोल सहित तमाम उदाहरण दिये जा सकते हैं।
जब जब एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं तब तब यह भी चर्चा जोर पकड़ती है कि क्या एक्ज़िट पोल प्रायोजित होते हैं या उन्हें शेयर बाजार या सट्टा मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसके अलावा यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जब चुनाव परिणाम कुछ दिनों में घोषित होने ही वाले होते हैं, तो फिर एक्ज़िट पोल की ज़रूरत ही क्या है? इसलिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
लोकतंत्र में Exit Poll क्यों महत्वपूर्ण हैं?
लोकतंत्र में मतदाता अपने मत डालते हैं। उन्होने किसी पार्टी को अपना वोट क्यों दिया यह समझने का सबसे सटीक तरीका एक्ज़िट पोल हैं। अक्सर, हम देखते हैं कि चुनावी चर्चाओं में सतही मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन कई एक्ज़िट पोल से पता चलता है कि लोगों की प्राथमिक चिंताएँ उनकी बुनियादी आवश्यकताएँ होती हैं। चुनाव परिणाम केवल हमें विजेता के बारे में तो बताते हैं, लेकिन उसके पीछे के कारण नहीं बताते। एक्ज़िट पोल पोल समाज में लोकतांत्रिक भावना को समझने के लिए आवश्यक हैं। वे सामाजिक विज्ञान शोध और लोकतंत्र तथा इसकी संस्थाओं के गहन अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण डेटा-आधारित जानकारी प्रदान करते हैं।
Exit Poll गलत होने से क्या होता है
एक्ज़िट पोल में होने वाली गंभीर गलतियाँ कई कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं। कई चुनाव विश्लेषकों कहते है कि हम अक्सर आम जनता की राय को सही ढंग से समझने में विफल रहते हैं। वहीं, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि आम लोग सर्वेक्षणकर्ताओं को ईमानदारी से अपनी राय देने में हिचकिचाते हैं। ये संभावित परिस्थितियाँ लोकतंत्र के नब्ज मापने के कार्य को चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। यदि जनता की असल राय को सटीक रूप से नहीं आंका जा सकता, तो यह एक सामाजिक समस्या बन सकती है। यदि एक्ज़िट पोल, जो कि शोध का एक प्रमुख तरीका है, बड़े पैमाने पर गलत साबित होते हैं, तो उनकी त्रुटियाँ चुनाव परिणाम आने के साथ ही स्पष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा, चुनावी प्रक्रिया में कई अन्य हितधारक शामिल होते हैं, जैसे कि नेता, मीडिया कर्मी, राजनीतिक दल और चुनाव विश्लेषक, जो इन गलतियों को पहचान लेते हैं। लेकिन कई दूसरे सामाजिक सर्वेक्षणों में यह संभव नहीं होता है।
जो तकनीक एग्जिट पोल में इस्तेमाल होती है वही पद्धति अन्य सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों में भी उपयोग की जाती है। यदि यह प्रक्रिया जनता की नब्ज़ समझने में विफल होती है, तो सामाजिक अध्ययनों के तहत किए गए सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी एजेंसी का एक्ज़िट पोल गलत साबित होता है, तो यह चुनाव परिणाम के दिन स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यदि कोई सामाजिक अध्ययन, जैसे शिक्षा की स्थिति को मापने वाला ASER सर्वेक्षण, त्रुटिपूर्ण हो, तो इसकी सटीकता का मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार, यदि एक्ज़िट पोल की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अन्य प्राथमिक शोध आधारित सर्वेक्षण भी संदेह के घेरे में आ सकते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतिगत निर्णय और उनके कार्यान्वयन में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
Exit Poll गलत क्यों होते हैं
गलत भविष्यवाणियों के पीछे के कारणों को समझने हेतु हमें चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों और उनके जटिल चरणों का विश्लेषण करना होगा। एक्ज़िट पोल यादृच्छिक (random) रूप से चुने गए मतदाताओं के नमूने से वोट शेयर का अनुमान लगाते हैं और फिर इसे सीटों की भविष्यवाणी में बदलने का प्रयास करते हैं। छोटे नमूनों से राष्ट्रीय परिणामों का अनुमान लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर जब मतदाता अपनी वास्तविक पसंद बताने में हिचकिचाते हैं।
आदर्श स्थिति में, सर्वेक्षण सैंपल की संरचना उस समुदाय की जनसांख्यिकी (demographics) को सही ढंग से दर्शानी चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 18% अल्पसंख्यक, 20% अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST), और 35% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हैं, तो उस क्षेत्र के सर्वेक्षण सैंपल में भी इन्हीं अनुपातों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके अलावा, लिंग (gender), शहरी और ग्रामीण जनसंख्या जैसे कारकों को भी सावधानीपूर्वक संतुलित करना आवश्यक है। हालाँकि, कई बार सर्वेक्षण एजेंसियाँ बड़े सैंपल साइज को जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व और यादृच्छिकता (randomness) जैसे महत्वपूर्ण तत्वों से अधिक महत्व देती हैं, जिससे सटीकता प्रभावित होती है।
अधिकतर मामलों में, समाज के प्रभावशाली वर्गों का प्रतिनिधित्व सैंपल में अधिक होता है (जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा या 2024 हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस), जबकि हाशिए पर मौजूद वर्गों का प्रतिनिधित्व आम तौर पर कम होता है। यह गलत प्रतिनिधित्व जानबूझकर नहीं किया जाता, बल्कि उस सामाजिक संरचना के कारण होता है जिसमें शोध किया जा रहा होता है। आम तौर पर प्रभावशाली समूह अधिक मुखर होते हैं, जबकि हाशिए के समुदाय अक्सर ‘मौन मतदाता’ होते हैं। चुनावी परिदृश्य में, मतदाताओं में एक प्रवृत्ति होती है कि वे ऐसे दल को वोट नहीं देते जिसे वे हारता हुआ मानते हैं। इसके परिणामस्वरूप, गुणात्मक (qualitative) रूप से अधूरे आंकड़े मिलते हैं, जिससे हाशिए के वर्गों के ‘स्विंग वोट’ का सटीक पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है।
इसके अलावा, प्रभावशाली समूहों के राजनीतिक विमर्श में दबदबे के कारण, एक्ज़िट पोल के आंकड़े तैयार करते समय “मुझे नहीं पता” या “कुछ नहीं कह सकते” जैसे अनिर्णीत उत्तरों को अक्सर मजबूत पार्टी के पक्ष में जोड़ दिया जाता है। इससे सर्वेक्षण के गलत साबित होने की संभावना बढ़ जाती है।
एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस पर ध्यान नहीं दिया हाता है कि क्या सर्वेक्षणकर्ताओं की टीम समाज का समानुपातिक प्रतिनिधित्व करती है या नहीं। कई मामलों में, सर्वेक्षणकर्ता शहरी, उच्च शिक्षित, उच्च वर्गीय, या पुरुष होते हैं। यदि सर्वेक्षण दल में महिलाओं, ग्रामीण व्यक्तियों और हाशिए के समुदायों के लोगों को शामिल किया जाए, तो सामाजिक सर्वेक्षण अधिक प्रभावी हो सकते हैं। हालाँकि, इस समस्या की पहचान करना तुलनात्मक रूप से आसान है, लेकिन किसी भी पोलिंग एजेंसी के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पाना एक जटिल प्रक्रिया है।
भारत की फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली में, करीबी चुनावी मुकाबलों की सटीक भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके अलावा, डिजिटल युग के आगमन के बाद गोपनीयता (privacy) को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण मतदाता अपनी पसंद बताने में झिझकते हैं।
फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली में बुनियादी आवश्यकता वोट शेयर को सटीक रूप से मापना है। सीटों में वोट शेयर को बदलना एक अलग प्रक्रिया है, जो सर्वेक्षण विज्ञान का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि ब्रिटेन जैसे कई देशों में केवल वोट शेयर की रिपोर्टिंग की जाती है, सीटों की नहीं। एजेंसियों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उनके आंकड़े वोट शेयर, मुद्दों और लोकप्रियता के संदर्भ में सटीक हैं, लेकिन वोट शेयर को सीटों में बदलने में वे पूरी तरह सही नहीं हो सकते। दुर्भाग्यवश, भले ही वोट शेयर सटीक हो, फिर भी अधिकतर लोग सीटों की संख्या की रिपोर्टिंग पर ज़ोर देते हैं।
सुधार की आवश्यकता
भारत में एग्जिट पोल की सटीकता और पारदर्शिता में सुधार के लिए नियम संबन्धित उपायों और शोध पद्धतियों दोनों में सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान में, एग्जिट पोल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A के तहत किए जाते हैं, जिसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए विशिष्ट दिशा-निर्देश हैं, ताकि उन्हें चुनावों को गलत तरीके से प्रभावित करने से रोका जा सके। हालाँकि, मतदान विधियों, सैंपलिंग तकनीकों और तकनीकी प्रगति में भिन्नताओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की एक श्रृंखला को संबोधित करने के लिए इन विनियमों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया जा सकता है।
विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणालियों में विविधता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ एजेंसियाँ फ़ोन सर्वेक्षण करती हैं, जबकि अन्य व्यक्तिगत फ़ील्डवर्क के माध्यम से डेटा एकत्र करती हैं। दृष्टिकोण में ये अंतर अत्यधिक अलग तरह के परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, जो अधिक मानकीकृत और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्रक्रिया की आवश्यकता को उजागर करता है। सैंपलिंग रणनीतियों और प्रश्नावली डिज़ाइन सहित कार्यप्रणाली को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से प्रत्येक सर्वेक्षण की ताकत और सीमाओं की स्पष्ट समझ हो सकेगी। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता न केवल विश्वास बढ़ाती है बल्कि जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि मतदाता और राजनीतिक विश्लेषक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि भविष्यवाणियाँ कैसे निकाली जाती हैं। इसके अलावा, जिस तरह व्यवसायों और सेवाओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसी तरह एग्जिट पोल कंपनियों के लिए चुनाव आयोग या केंद्र सरकार के किसी निकाय द्वारा पर्यवेक्षित पंजीकरण और विनियमन प्रक्रिया से गुजरना फायदेमंद हो सकता है। लाइसेंसिंग से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि केवल योग्य, निष्पक्ष एजेंसियां ही पोल करें, जिससे हेरफेर की संभावना कम हो तथा डेटा की विश्वसनीयता बढ़े। अधिक पारदर्शिता के लिए, एग्जिट पोल एजेंसियों को कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना चाहिए, जैसे कि स्वामित्व का विवरण, प्रायोजन की प्रकृति और स्रोत, मतदाता जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, प्रश्न डिज़ाइन और वो प्रक्रिया जिसके द्वारा वोट शेयर डेटा को सीट अनुमानों में परिवर्तित किया जाता है। जब ये तत्व स्पष्ट हो जाते हैं, तो जनता बेहतर ढंग से समझ सकती है कि भविष्यवाणियां कैसे उत्पन्न होती हैं, और सर्वेक्षण एजेंसियों को जवाबदेही के उच्च मानक पर रखा जाता है। अन्य लोकतंत्रों के उदाहरण हैं जिनका भारत अनुसरण कर सकता है। कई यूरोपीय और अमेरिकी देशों में एग्जिट पोल प्रसारण के समय पर सख्त नियम हैं। इससे अनिर्णीत मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव को रोकने में मदद मिलती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत एग्जिट पोल की वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा को और बढ़ाने के लिए इसी तरह के उपाय अपना सकता है।
वर्तमान में चुनाव आयोग के पास अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव प्रथाओं को रेगुलेट करने का अधिकार है, लेकिन प्रेस काउंसिल या न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के अतिरिक्त नियम मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एग्ज़िट पोल के लिए एक सुसंगत और विश्वसनीय मानक बनाने में मदद कर सकते हैं। किसी भी सर्वेक्षण का संचालन करने से पहले, सर्वेक्षणकर्ताओं को मतदाताओं से सावधानीपूर्वक संपर्क करना चाहिए, वोट शेयर और अन्य जनसांख्यिकीय डेटा इकट्ठा करने के लिए सवाल पूछना चाहिए जो सटीक आकलन करने की अनुमति देगा। सर्वेक्षण एजेंसियों के लिए नई, अधिक सटीक पद्धतियों को अपनाने की भी आवश्यकता है। सर्वे एजेंसियां सटीकता और वैज्ञानिक पद्धति पर ध्यान देकर, बिना किसी दबाव में आए, डेटा के आधार पर मतदाताओं की प्राथमिकताओं की स्पष्ट जानकारी दे सकती हैं।
राजनीती और चुनाव से जुड़े और आर्टिकल पढ़े – Vichar Darpan | Politics